जीवन परिचय-
लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से सम्बन्धित प्रामाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। डॉ० नगेन्द्र द्वारा लिखित ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में उनके सन्दर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं- बेनीमाधव प्रणीत ‘मूल गोसाईंचरित’ तथा महात्मा रघुबरदास रचित ‘तुलसीचरित’ में तुलसीदासजी का जन्म संवत् 1554 वि० (सन् 1497 ई०) दिया गया है। बेनीमाधवदास की रचना में गोस्वामीजी की जन्म-तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है-
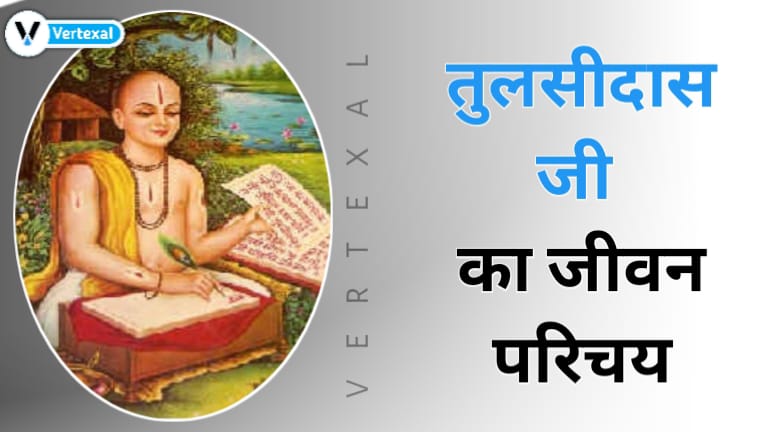
पंद्रह सौ चौवन बिसै, कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो सरीर।।
‘शिवसिंह सरोज’ में इनका जन्म संवत् 1583 वि० (सन् 1526 ई०) बताया गया है। पं० रामगुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत् 1589 वि० (सन् 1532 ई०) स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत् को मान्यता दी गई है। निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म संवत् 1589 वि० (सन् 1532 ई०) माना जाता है।
इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद हैं। \’तुलसी-चरित\’ में इनका जन्मस्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले का एक गाँव है। कुछ विद्वान् तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति “मैं पुनि निज गुरु सन सुनि, कथा सो सूकरखेत\” के आधार पर इनका जन्मस्थल एटा जिले के ‘सोरो’ नामक स्थान को मानते है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ‘सूकरखेत’ को भ्रमवश ‘सोरो’ मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्मस्थान को राजापुर माननेवाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है।
जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दूबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता-पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन-पोषण प्रसिद्ध सन्त बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण-कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना की, जिससे ये प्रभु-भक्ति की ओर उन्मुख हो गए।
संवत् 1680 ( सन् 1623 ई० ) में, काशी में इनका निधन हो गया।
साहित्यिक परिचय-
महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान् लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा-निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य ‘श्रीरामचरितमानस’, भाषा, भाव, उद्देश्य, कथावस्तु, चरित्र-चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का एक अद्भुत ग्रन्थ है। इसमें तुलसी के कवि, भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। ‘श्रीरामचरितमानस’ में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ-प्रदर्शन करता रहा है। ‘विनयपत्रिका’ ग्रन्थ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त-हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। इसमें एक भक्त के रूप में तुलसी ईश्वर के प्रति दैन्यभाव से अपनी व्यथा-कथा कहते हैं
गोस्वामी तुलसीदास की काव्य-प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये समन्वयवादी थे। इन्होंने’श्रीरामचरितमानस’ में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव सम्प्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। निषाद एवं शबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज की जातिवाद पर आधारित भावना की निस्सारता (महत्त्वहीनता) को प्रकट किया और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया।
संक्षेप में तुलसीदास एक विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न तथा लोकहित एवं समन्वय भाव से युक्त महाकवि थे। भाव-चित्रण, चरित्र-चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्श के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण सम्पूर्ण विश्व-साहित्य में भी मिलना दुर्लभ है।
कृतियाँ-
- ‘श्रीरामचरितमानस’,
- ‘विनयपत्रिका’,
- ‘कवितावली’,
- ‘गीतावली’,
- ‘श्रीकृष्णगीतावली’,
- ‘दोहावली’,
- ‘जानकी-मंगल’,
- ‘पार्वती-मंगल’,
- ‘वैराग्य-सन्दीपन’
- तथा ‘बरवै-रामायण’ आदि।
हिन्दी-साहित्य में स्थान –
वास्तव में तुलसी हिन्दी-साहित्य की महान् विभूति हैं। उन्होंने रामभक्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित करके जन-जन का जीवन कृतार्थ कर दिया। उनके साहित्य में रामगुणगान, भक्ति-भावना, समन्वय, शिवम् की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, जो उन्हें महाकवि के आसन परप्रतिष्ठित करती हैं। महाकवि हरिऔधजी ने सत्य ही लिखा है कि तुलसी की कला का स्पर्श प्राप्तकर स्वयं कविताही सुशोभित हुई है-
